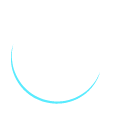झारखंड 'वनों की भूमि' होने के अलावा विरोधाभासों की भी भूमि है। पूर्वी भारत के इस हिस्से की मिट्टी खनिज से समृद्ध है, खेती के लिए उपजाऊ है। लेकिन अस्थिर मानसून और सूखे की वजह से ये सारी संभावनाएं धरी की धरी रह जाती हैं।
राज्य में कई गांव दूरस्थ इलाकों में हैं, जहां किसान बेहद सीमित संसाधनों और पुराने कृषिगत औजारों के साथ छोटी सी खेतिहर ज़मीन पर महज़ निर्वाह लायक खेती करते हैं। गांव वाले सिर पर सब्ज़ियों और लकड़ियों का गट्ठर उठाए खेतों के बीच संकरी पगडंडियों पर चलते हैं, और ज़मीन से ही अपनी आजीविका कमाते हैं।
झारखंड के गुमला जिले में, एक छोटे से सामुदायिक केंद्र पर बड़ी चहल-पहल है। अंदर, सभी उम्र की औरतें, जिनमें से कुछ औरतों की गोद में बच्चे हैं, यहां एक उत्पादक समूह की बैठक के लिए इकट्ठा हुई हैं।
बाहर, चारों तरफ़ बैंगन, दालों और टमाटरों की हरी-भरी कतारों के खेत दिखाई देते हैं, जो इन महिलाओं की कड़ी मेहनत की गवाही देते हैं। ये महिलाएं अपनी सब्ज़ियों को बाज़ार तक पहुंचाने की रणनीतियों पर चर्चा कर रही हैं। ये फसलें योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई हैं ताकि जब सोहराय आए तो भोज एवं अनुष्ठानों के लिए इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सोहराय फसल कटाई का एक उत्सव है जिसे अक्टूबर-नवंबर के महीने में मनाया जाता है।
इन महिलाओं के लिए यह बैठक केवल फसल कटाई के लिए नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और मज़बूत भविष्य का सपना लिए वे यहां इकट्ठा हुई हैं।
राज्य भर के क़रीब 2 लाख परिवारों की तरह, ये औरतें 'जोहार' (झारखंड ऑपर्च्युनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ) कार्यक्रम के ज़रिए अपनी आजीविका में बदलाव ला रही हैं।
इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसके कार्यान्वयन में सहयोग देने तक, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के इन्वेस्टमेंट सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सहयोग के तहत कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश किया गया और महिलाओं की बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाया गया है।
झारखंड सरकार के ग्रामीण विभाग के नेतृत्व में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज (जेएसएलपीएस) के तहत कार्यान्वित किए जा रहे जोहार कार्यक्रम की मदद से 1.5 लाख से ज्यादा परिवार निर्वाह लायक धान की खेती छोड़कर उच्च मूल्य वाली कृषि की ओर मुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक का वित्तीय समर्थन प्राप्त है।
अब ये परिवार लाभदायक फसलें जैसे फल और सब्जियां उगाते हैं और साथ ही पशुपालन से भी आय अर्जित करते हैं। इनमें से कई परिवारों की आमदनी में 35 प्रतिशत से अधिक का इज़ाफ़ा हुआ है।
यह जोहार कार्यक्रम की ही बदौलत है कि सिर्फ़ चार सालों में महिला नेतृत्व वाले 21 किसान उत्पादक संगठनों ने लगभग 2.1 करोड़ डॉलर का कारोबार किया है, जिनसे क़रीब 4000 उत्पादक समूह से जुड़े हुए हैं। किसानों को इसका सीधा फायदा हुआ है। वे खुले बाज़ार से भी कम कीमत पर कृषि सामग्री खरीदते हैं और अपनी उपज किसान उत्पादक संगठनों को बेचकर बेहतर लाभ कमाते हैं।
इन उत्पादक समूहों की औरतों के लिए इसका मतलब है कि उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं और उनकी आजीविका और सुरक्षित हो गई है। उनकी सफलता हमें यह बताती है कि झारखंड के किसानों को अगर सही संसाधन मिलें तो वे कृषि में परिवर्तनकारी बदलाव की ताकत रखते हैं।