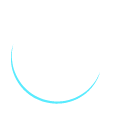अनीता देवी का परिवार उत्तराखंड के देहरादून में ऐसे ही एक इलाके में रहता है। तीस साल पहले जब उनकी शादी हुई थी उसके बाद से ही अनीता रोजाना पानी इकट्ठा करने की तकलीफ़ से गुजरती रही हैं। अनीता याद करते हुए कहती हैं, “हमारे लिए पानी की समस्या कभी न ख़त्म होने वाली थी। हमें या तो पहाड़ की चोटी से पानी लाना पड़ता था या नीचे बहती नदी से।" ज्यादातर बार उन्हें अपने बच्चों से मदद लेनी पड़ ती थी जिससे वे स्कूल देर से पहुंचते थे।
इसके बावजूद, उनके परिवार की जरूरतों या पालतू गाय के लिए ये पानी कभी भी पर्याप्त नहीं होता था।
उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहर, जो तीव्र शहरीकरण से गुजर रहे हैं, वहां भी सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे थे। लोगों को हर दिन सरकारी टैंकरों के सामने पानी भरने के लिए लाइन में घंटों तक खड़ा रहना पड़ ता था। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, वे महंगे दामों पर पानी खरीदते थे या फिर खुद का बोरवेल खुदवाने में भारी खर्च करते थे। जिनके घरों में नगर निगम की पाइपलाइन से कनेक्शन था, उन्हें भी पानी को पंप करके उसके भंडारण और शुद्धि करण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। पानी की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और उसकी आपूर्ति भी अनियमत रहती थी।
अच्छी बात यह है कि अब हालात बदल रहे हैं। आज अनीता देवी के घर में पानी का कनेक्शन है, जो उन्हें हर दिन 16 से 24 घंटे तक साफ़ पानी उपलब्ध कराता है। उन्होंने खुश होकर बताया, "अब हमें न तो नदी तक जाना पड़ता है, न ही टैंकर का इंतज़ार करना पड़ता है, और न ही पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है।”